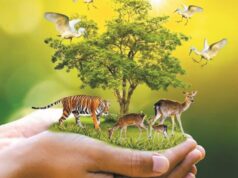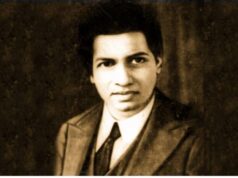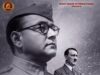(संदीप सृजन-विनायक फीचर्स)
भारत की गौरवशाली वांग्मय परम्परा के प्रमुख दर्शन जैन दर्शन और वैदिक दर्शन, दोनों ही भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं के प्रमुख स्तंभ हैं, जो क्षमा को आत्म-उन्नति का माध्यम मानते हैं। जैन दर्शन में क्षमा अहिंसा का अभिन्न अंग है, जबकि वैदिक दर्शन में यह धर्म और मोक्ष का आधार है। क्षमा भावना मनुष्य में देवत्व की प्रतिष्ठा करती है यह कथन मानव जीवन की गहन सत्यता को उजागर करता है। क्षमा, जो क्रोध, द्वेष और प्रतिशोध की जंजीरों से मुक्त करती है, मनुष्य को उसकी आंतरिक दिव्यता की ओर ले जाती है। क्षमा कोई कमजोरी नहीं, बल्कि शक्ति का प्रतीक है। जैन और वैदिक ग्रंथों में क्षमा को आत्म-शुद्धि का साधन माना गया है। जैन दर्शन में यह कर्म-बंधन से मुक्ति का मार्ग है, जबकि वैदिक परंपरा में यह ब्रह्म-ज्ञान की प्राप्ति का माध्यम।
जैन दर्शन, जो अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांतवाद पर आधारित है। क्षमा यहां अहिंसा का विस्तार है। जैन ग्रंथों जैसे ‘उत्तराध्ययन सूत्र’ और ‘तत्वार्थ सूत्र’ में क्षमा को ‘क्षांति’ कहा गया है, क्षांति का अर्थ है सहनशीलता और क्षमा। जैन मतानुसार, मनुष्य का जीवन कर्मों से बंधा है। क्रोध और द्वेष जैसे विकार नए कर्मों को आकर्षित करते हैं, जो आत्मा को जन्म-मरण के चक्र में बांधते हैं। क्षमा इन विकारों को नष्ट करती है, और आत्मा को कैवल्य (मोक्ष) की ओर ले जाती है।
जैन दर्शन में क्षमा को ‘सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चरित्र’ के त्रिरत्नों के अंतर्गत रखा गया है।
उदाहरणस्वरूप, महावीर स्वामी ने अपने जीवन में अनेक कष्ट सहे, लेकिन कभी प्रतिशोध नहीं लिया। जब एक सर्प ने उन्हें डसा, तो उन्होंने क्षमा भाव से कहा, “यह इसका कर्म है।” यह घटना दर्शाती है कि क्षमा मनुष्य को देवत्व प्रदान करती है, क्योंकि देवता क्रोध से मुक्त होते हैं। जैन साहित्य में ‘प्रतिक्रमण’ अनुष्ठान है, जिसमें व्यक्ति अपने पापों के लिए क्षमा मांगता है। यह अनुष्ठान आत्म-शुद्धि का माध्यम है। जैन दर्शन क्षमा को चार प्रकारों में वर्गीकृत करता है: क्रोध न करना, क्रोध होने पर उसे नियंत्रित करना, अपराधी को क्षमा करना, और स्वयं को क्षमा करना। ‘आचारांग सूत्र’ में वर्णित है कि क्षमा से जीव अहिंसा का पालन करता है, जो सभी जीवों के प्रति समानता का भाव जगाता है।
क्षमा जैन दर्शन में सामाजिक सद्भाव का भी साधन है। जैन समाज में क्षमा के माध्यम से संघर्षों का समाधान किया जाता है। उदाहरण के लिए, जैन मुनि कभी विवाद में नहीं पड़ते, वे क्षमा भाव अपनाते हैं। यह दर्शन बताता है कि मनुष्य जन्म से देव नहीं होता, लेकिन क्षमा जैसे गुणों से देवत्व अर्जित कर सकता है। जैन दर्शन की यह शिक्षा आज के संघर्षपूर्ण विश्व में प्रासंगिक है, जहां क्षमा शांति का मार्ग प्रशस्त करती है।
वैदिक दर्शन, जो वेदों, उपनिषदों, पुराणों और स्मृतियों पर आधारित है, क्षमा को ‘क्षमा’ या ‘तितिक्षा’ के रूप में वर्णित करता है। ऋग्वेद में कहा गया है: “क्षमां भूमि: क्षमां जलं, क्षमां वायु: क्षमां आकाशं” अर्थात क्षमा पृथ्वी, जल, वायु और आकाश की तरह अनंत है। वैदिक मतानुसार, मनुष्य ब्रह्म का अंश है, लेकिन माया और अविद्या से ढका हुआ। क्षमा इन आवरणों को हटाती है, और आत्मा को ब्रह्म से एकाकार करती है, जो देवत्व है।
वैदिक दर्शन में क्षमा को धर्म का अभिन्न भाग माना गया है। मनुस्मृति में लिखा है: “क्षमा धर्म का मूल है।” क्षमा से मनुष्य अपने विकारों पर विजय प्राप्त करता है, और देवत्व की ओर बढ़ता है। उपनिषदों में, जैसे बृहदारण्यक उपनिषद में, क्षमा को ‘तप’ का रूप कहा गया है। वैदिक दर्शन में क्षमा ‘कर्म योग’ का भाग है, जहां कर्म फल की अपेक्षा न करके क्षमा की जाती है। यह भावना मनुष्य को उसके अहंकार से मुक्त करती है, और ब्रह्म-ज्ञान प्रदान करती है।
जैन और वैदिक दर्शन दोनों ही क्षमा को आत्म-उन्नति का साधन मानते हैं, दोनों दर्शन क्षमा को विकार-नाशक मानते हैं। जैन के ‘क्षांति’ और वैदिक के ‘तितिक्षा’ समान हैं। दोनों में क्षमा मोक्ष का मार्ग है। क्षमा भावना मनुष्य में देवत्व की प्रतिष्ठा करती है, जैसा जैन और वैदिक दर्शन सिखाते हैं। जैन में यह अहिंसा का फल है, वैदिक में धर्म का। दोनों से प्रेरणा लेकर, हम क्षमा अपनाकर दिव्य जीवन जी सकते हैं। क्षमा से ही विश्व शांति संभव है। अंत में, क्षमा अपनाएं, देवत्व प्राप्त करें। (विनायक फीचर्स)